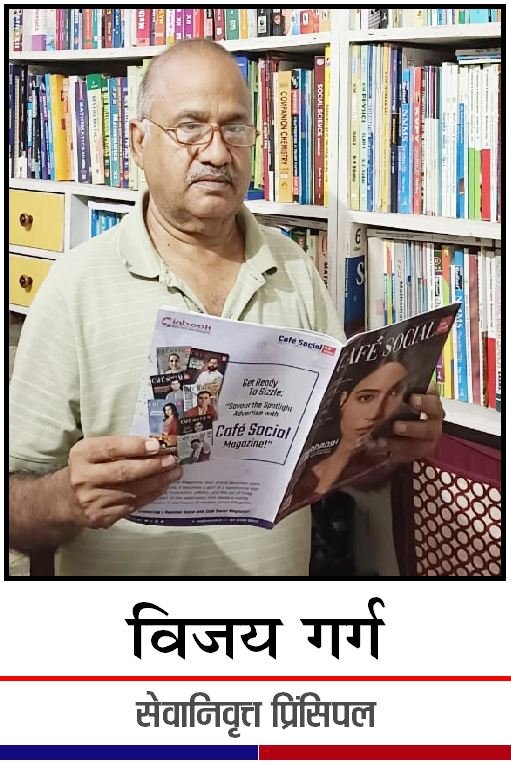डॉ विजय गर्ग
समकालीन समाज तेजी से बदल रहा है। हर दिन अखबारों और डिजिटल माध्यमों में पीड़ा, असमानता और संघर्ष की खबरें आम हो गई हैं। आदिवासी अंचलों में विस्थापन, शहरों की ओर बढ़ता पलायन, शिक्षा से बाहर होते बच्चे और महिलाओं के साथ होती हिंसा – ये अब केवल घटनाएं नहीं, बल्कि आंकड़ों में दर्ज सच्चाइयां हैं। इन पर हम दुख व्यक्त करते हैं, सहानुभूति जताते हैं, लेकिन हमारा सामाजिक आचरण अक्सर वहीं
ठहर जाता है।
किसी के दुख को देखकर करुणा का भाव जागना समाज को असंवेदनशील होने से बचाता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह भावना केवल शब्दों, बयानों और औपचारिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित रह जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित सामाजिक और आर्थिक रपटें बताती हैं कि असमानता और वंचना आज भी व्यापक है, फिर भी अधिकांश मामलों में हमारी भूमिका केवल चिंता व्यक्त करने तक सिमट जाती है। असल में सहानुभूति हमें भावनात्मक संतोष देती है, पर व्यावहारिक जिम्मेदारी का बोध नहीं कराती ।
आदिवासी समाज इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 फीसद हिस्सा अनुसूचित
जनजातियों का है, लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में उनकी हिस्सेदारी अनुपात से कहीं अधिक रही है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बड़े बांधों, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों में लगभग चालीस फीसद तक आदिवासी समुदायों से आते हैं। यह तथ्य केवल विस्थापन का नहीं, बल्कि संस्कृति, आजीविका और सामाजिक पहचान के टूटने का भी संकेत देता है। सहानुभूति के रूप में मुआवजे और पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन समानुभूति तभी होगी, जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और विकास
को उनके जीवन-संदर्भ से जोड़कर देखा जाए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी यही अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। यूनिसेफ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं की रपटें बताती हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अब भी चिंता का विषय है, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में। सहानुभूति के तौर पर छात्रवृत्तियां, मध्याह्न भोजन और योजनाएं मौजूद हैं, पर समानुभूति तब सामने आती है जब शिक्षा व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि भाषा, गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियां सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जब शिक्षक और व्यवस्था बच्चे की पृष्ठभूमि को समझकर अपनी पद्धति में बदलाव करते हैं, तभी शिक्षा वास्तव में
समावेशी बनती है।
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन भी हमारे सामाजिक आचरण की परीक्षा लेता है। करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहरों में अस्थायी या असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। शहरी अर्थव्यवस्था इन श्रमिकों पर निर्भर है, फिर भी सामाजिक व्यवहार में वे अक्सर अदृश्य रहते हैं। हम उनके श्रम का लाभ उठाते हैं, पर उनके आवास, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर उदासीन बने रहते हैं। यह उदासीनता सहानुभूति की सीमा को दर्शाती है, जहां समस्या को देखा तो जाता है, पर उसे अपना नहीं
माना जाता।
डिजिटल युग ने संवेदनाओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती । असल में केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं, जब तक सामाजिक और मानवीय दृष्टि उसके साथ न चले। सामाजिक आचरण तब बदलता है, जब संवेदना औपचारिकता से निकलकर व्यवहार उतरती है। जब नीति निर्माण में आंकड़ों के साथ मानवीय अनुभवों को महत्त्व दिया जाता है, जब योजनाएं बनाते समय जमीनी सच्चाइयों को समझा जाता है, तब सहानुभूति समानुभूति में बदलती है।
डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब