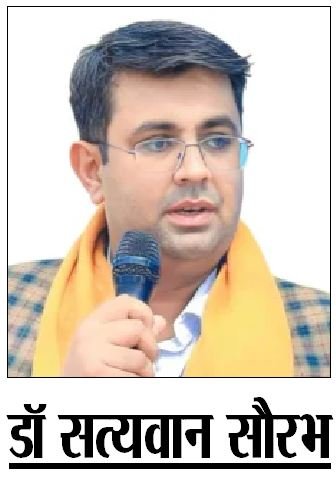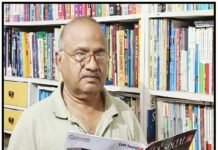– डॉ सत्यवान सौरभ
“वंदे मातरम्” भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आध्यात्मिक आधार था। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि को देवी के रूप में पूजने की भावना से ओतप्रोत था। इसने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि एक भक्ति-भावना में परिवर्तित किया। बंग-भंग आंदोलन से लेकर क्रांतिकारी संघर्षों तक यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बना। आज भी यह राष्ट्रीय सम्मान, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। “वंदे मातरम्” ने भारत की आत्मा को जागृत किया और यह सदा हमारी राष्ट्रीय चेतना की धड़कन बना रहेगा।
“वंदे मातरम्” केवल एक गीत नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र की आत्मा का स्वर बन गया। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उनकी प्रसिद्ध कृति आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया था। इसमें भारत माता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने औपनिवेशिक दमन से त्रस्त भारतीय जनमानस को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा। इस गीत ने न केवल भावनात्मक स्तर पर भारतीयों को जोड़ा बल्कि स्वतंत्रता की मांग को एक नैतिक और धार्मिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। यह वह समय था जब भारत अंग्रेज़ी शासन के अधीन था, और समाज निराशा, विभाजन तथा अधीनता की मानसिकता में जी रहा था। ऐसे में “वंदे मातरम्” ने भारतवासियों के भीतर दबी हुई स्वाभिमान की चिंगारी को प्रज्वलित किया।
इस गीत की पहली दो पंक्तियाँ—“सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् शस्यश्यामलाम् मातरम्”—भारत की भौगोलिक सुंदरता और समृद्धि का वर्णन करती हैं। यहाँ भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी माँ के रूप में चित्रित की गई है जो अपने बच्चों को जल, अन्न और जीवन देती है। यह भावनात्मक रूपक उस समय के लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी था। भारतीय समाज के लिए मातृत्व का भाव सबसे पवित्र था, और जब देश को ‘मां’ के रूप में देखा गया, तो देशभक्ति स्वाभाविक रूप से ‘भक्ति’ का रूप ले ली। यह भाव ही “वंदे मातरम्” को एक साधारण गीत से एक आध्यात्मिक आंदोलन में परिवर्तित करता है।
भारत में उस समय राजनीतिक चेतना का आरंभ हो रहा था, परंतु उसमें जनसामान्य की भागीदारी सीमित थी। शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हो रहे थे, लेकिन उनमें भावनात्मक ऊर्जा का अभाव था। “वंदे मातरम्” ने इस रिक्तता को भरा। इसने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप दिया। यह गीत गाया गया तो लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि वे किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं, बल्कि अपनी ही मातृभूमि के संतान हैं, जिन्हें स्वतंत्र रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है।
1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, तब “वंदे मातरम्” बंग-भंग आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। विद्यार्थी, महिलाएँ, व्यापारी, किसान—सबके होंठों पर यही शब्द गूंजने लगे। रैलियों, सभाओं और जुलूसों में जब यह गीत सामूहिक रूप से गाया जाता था, तो लोगों के भीतर अजेय शक्ति का संचार होता था। अंग्रेज़ सरकार को यह गीत इतना खतरनाक लगा कि उसने इसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद यह गीत और भी लोकप्रिय होता गया। स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों में गुप्त रूप से “वंदे मातरम्” गाया जाने लगा। यह गीत प्रतिरोध, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक बन चुका था।
भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां भाषा, धर्म और जाति के आधार पर समाज बँटा हुआ था, वहाँ “वंदे मातरम्” ने सबको एक सूत्र में बाँधने का कार्य किया। इस गीत ने सभी वर्गों को एक साझा सांस्कृतिक प्रतीक दिया—‘मां’। चाहे बंगाल हो, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु—हर प्रदेश ने इस गीत में अपनी मातृभूमि की छवि देखी। इसने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा आधार बनी।
“वंदे मातरम्” के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई भाषा और अभिव्यक्ति मिली। इसने राजनीतिक संघर्ष को धार्मिक उत्सव का रूप दे दिया। यह केवल विदेशी शासन के विरोध का प्रतीक नहीं था, बल्कि अपने भीतर के आत्मसम्मान को पहचानने का आह्वान भी था। इस गीत ने भारतीय समाज को यह बोध कराया कि पराधीनता केवल बाहरी शासन की नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी की भी जंजीर है। जब लोग मातृभूमि को देवी के रूप में पूजने लगे, तब स्वतंत्रता केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं रही, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन गई।
इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई महान नेताओं को गहराई से प्रभावित किया। श्री अरविंदो घोष ने कहा था कि “वंदे मातरम् वह मंत्र है जो हमें स्वराज्य की प्राप्ति तक ले जाएगा।” नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपने इंडियन नेशनल आर्मी का राष्ट्रीय गीत बनाया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जब जेल में जाते या फाँसी का सामना करते, तो उनके होंठों पर “वंदे मातरम्” होता। इसने युवाओं के भीतर बलिदान और वीरता की भावना को प्रबल किया।
सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह गीत भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक बना। उस समय रवींद्रनाथ ठाकुर, अबनिंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस जैसे कलाकार और लेखक भारतीय पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। “वंदे मातरम्” ने उन्हें एक साझा प्रेरणा दी। भारतीय चित्रकला, नाट्यकला, संगीत और साहित्य में मातृभूमि का रूपांकन इसी गीत से प्रभावित हुआ। यह वह काल था जब भारतीय संस्कृति अपने खोए गौरव को पुनः खोजने में लगी थी और “वंदे मातरम्” उसका सबसे प्रभावशाली प्रतीक बना।
ब्रिटिश शासन के लिए यह गीत विद्रोह का प्रतीक था। अंग्रेज़ इसे धार्मिक विभाजन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे, परंतु भारतीयों के लिए यह गीत किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का प्रतीक था। इसमें हिन्दू देवी-देवताओं के रूपक अवश्य थे, परंतु उसका उद्देश्य किसी धर्म को श्रेष्ठ बताना नहीं, बल्कि मातृभूमि को पवित्रता के स्तर पर प्रतिष्ठित करना था। यह गीत उस समय के सामाजिक-सांस्कृतिक मानस में राष्ट्र की नई परिभाषा गढ़ रहा था—एक ऐसी परिभाषा जिसमें धर्म से ऊपर देशभक्ति थी।
वंदे मातरम् की शक्ति उसकी सरलता और भावनात्मक गहराई में निहित थी। इसकी प्रत्येक पंक्ति भारत के सौंदर्य और गरिमा का बखान करती है। “त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी” जैसी पंक्ति ने यह संकेत दिया कि भारत की भूमि केवल कोमल नहीं, बल्कि शक्तिशाली भी है—जो अपने बच्चों की रक्षा करने में सक्षम है। इसने भारतीय नारी शक्ति और राष्ट्रशक्ति दोनों को एक रूप में देखने की प्रेरणा दी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब भी आंदोलन कमजोर पड़ता, “वंदे मातरम्” की गूंज लोगों में फिर से ऊर्जा भर देती। यह गीत लोगों के दिलों में इतना गहराई से बस गया कि यह स्वतंत्रता की प्रतीक ध्वनि बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे गाना परंपरा बन गई। महात्मा गांधी ने इसे भारत की आत्मा का गीत कहा। हालांकि कुछ धार्मिक समुदायों ने इसकी कुछ पंक्तियों पर आपत्ति की, फिर भी अधिकांश भारतीयों के लिए यह राष्ट्र की भावना का सर्वोच्च प्रतीक बना रहा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत का संविधान तैयार हुआ, तब “वंदे मातरम्” को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई, जबकि “जन गण मन” को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया। संविधान सभा की चर्चाओं में यह स्पष्ट किया गया कि “वंदे मातरम्” का सम्मान राष्ट्रगान के समान रहेगा, क्योंकि इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अनुपम योगदान दिया था।
आज भी जब यह गीत गाया जाता है, तो उसकी ध्वनि में वही जोश, वही भक्ति और वही मातृभाव झलकता है जो स्वतंत्रता सेनानियों के समय था। यह गीत हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल राजनीतिक सीमाओं का नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति, एक साझा भावना और एक आत्मा है जो हमें एक साथ जोड़ती है।
“वंदे मातरम्” ने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद के बीज बोए और उन्हें एक ऐसे वृक्ष में परिवर्तित किया जिसकी छाया में भारत ने स्वतंत्रता का फल पाया। इसने यह सिद्ध किया कि जब कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी मातृभूमि को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे लंबे समय तक दास नहीं बना सकती। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि भारतीय आत्मजागरण का गीत है।
इस गीत ने भारतीय जनमानस को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व भी है—अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि और अपने समाज के प्रति। “वंदे मातरम्” में गूंजती आवाज़ केवल एक कालखंड की नहीं, बल्कि युगों-युगों तक प्रेरणा देने वाली पुकार है। यह पुकार हमें बार-बार स्मरण कराती है कि राष्ट्र की सच्ची शक्ति उसकी एकता, उसकी आस्था और उसके स्वाभिमान में निहित है।
अंततः कहा जा सकता है कि “वंदे मातरम्” ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिशा दी। यह गीत भारतीय राष्ट्रीयता का वह ज्योति-पुंज बन गया जिसने अंधकारमय औपनिवेशिक काल में प्रकाश फैलाया। आज भी जब इसकी धुन बजती है, तो प्रत्येक भारतीय के भीतर एक अलौकिक गर्व, श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव जाग उठता है। यह केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है—जो हमें यह सिखाती है कि जब तक “वंदे मातरम्” की भावना जीवित है, भारत की आत्मा अमर है।