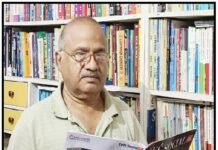प्रशांत कटियार
भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में तैयार होता है। 1964 में कोठारी आयोग ने यह वाक्य लिखा था, लेकिन शायद ही उसने सोचा होगा कि छह दशक बाद भी यह भविष्य उन्हीं कक्षाओं में गढ़ा जाएगा, जहाँ बच्चे तो हैं, पर मार्गदर्शन देने वाला शिक्षक अक्सर नदारद है। भीड़भरी कक्षाएँ बच्चों से भरी हैं, लेकिन उनमें वह प्रेरणा नहीं है, जो केवल शिक्षक की उपस्थिति से आती है। परिणाम यह है कि लाखों बच्चे बिना सही दिशा पाए अपनी और देश की तकदीर गढ़ने को विवश हैं।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट कहती है कि देश में एक करोड़ शिक्षक 24 करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुनने में यह अनुपात ठीक लगता है, लेकिन ज़मीनी तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का उदाहरण लें—यहाँ 1,32,855 सरकारी स्कूलों में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। औसतन हर स्कूल में 4–5 शिक्षक। लेकिन इसी के बीच 8,866 स्कूल ऐसे भी हैं, जहाँ पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी सिर्फ़ एक शिक्षक के कंधों पर है, और इन स्कूलों में छह लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। यानी अकेले एक शिक्षक को औसतन 70 से अधिक बच्चों को संभालना पड़ता है। यही स्थिति अन्य बड़े राज्यों में भी है। देश के 10 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में से 1 लाख से अधिक स्कूल आज भी “सिंगल-टीचर स्कूल” कहलाते हैं।
‘शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं’—यह कहावत आज के हालात में कहीं खो सी गई है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, देश में लगभग 10 लाख शिक्षकों की कमी है, जिनमें से 4 लाख पद तो प्राथमिक स्तर पर ही खाली हैं। इन रिक्तियों को भरना कठिन नहीं है, लेकिन समस्या इच्छाशक्ति और प्राथमिकता की है। शिक्षा नीति और भर्ती प्रक्रिया में लगातार बदलाव होते रहते हैं, पर स्पष्ट दृष्टि का अभाव है। नतीजा यह कि शिक्षक बनने के लिए किस तरह का प्रशिक्षण और योग्यता जरूरी है, इस पर कोई ठोस दिशा नहीं बन पाती।
शिक्षकों की सेवा शर्तें और वेतनमान भी बड़ी समस्या हैं। भर्ती में देरी, ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और नौकरी की असुरक्षा इस पेशे को युवाओं के लिए आकर्षक नहीं बनने देते। जब भविष्य गढ़ने वाले ही असमानता और असुरक्षा से जूझ रहे हों, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा?
नीति-निर्माताओं ने सुधार के नाम पर जो नए प्रयोग किए हैं, वे भी शिक्षकों का बोझ बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पेशेवर मानक (NPST) या हर वर्ष 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण (CPD) जैसी व्यवस्थाएँ व्यवहार में नौकरशाही का अतिरिक्त भार बनकर सामने आ रही हैं। इससे शिक्षकों की स्वायत्तता और मनोबल, दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
जरूरत इस बात की है कि शिक्षकों को केवल भावुक भाषा में “राष्ट्र निर्माता” कहने के बजाय वास्तविक सम्मान और गरिमा दी जाए। जब तक उन्हें पेशेवर स्वायत्तता और सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक वे मात्र आदेश पालन करने वाले कर्मचारी बने रहेंगे।
इक्कीसवीं सदी में शिक्षक होना न सिर्फ चुनौती है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी है। तकनीक बच्चों तक जानकारी पहुँचा सकती है, लेकिन उसे प्रेरणा और जीवन की दिशा में बदलने का काम केवल शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक और व्यक्तित्व निर्माता है, जो विद्यार्थियों को सोचने और सवाल करने की शक्ति देता है।
अगर हमने इस क्षमता में निवेश नहीं किया, तो भविष्य की पीढ़ी बिना मार्गदर्शन के उलझन और भ्रम की दुनिया में पनपेगी—और तब वास्तव में वह पंक्ति डरावनी हकीकत बन जाएगी कि “भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है”, लेकिन बिना शिक्षक के।